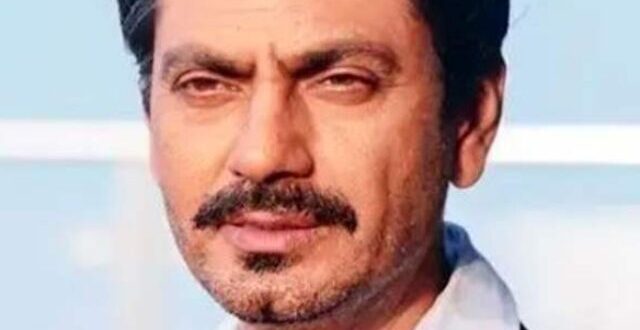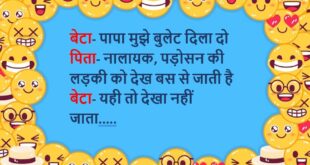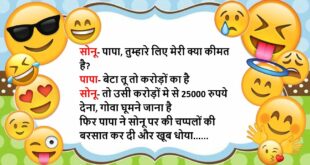साल 2015 की बात है, जब केतन मेहता की फिल्म ‘मांझी – द माउंटेन मैन’ के प्रमोशन के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उस इंटरव्यू में नवाज ने अपनी किशोरावस्था के सिनेमा अनुभव को साझा करते हुए बताया था कि उन्होंने सी-ग्रेड फिल्मों के बीच अपनी सिनेमाई समझ विकसित की।
उन्होंने कहा – “मैं जिस कस्बे (मुज़फ्फरनगर) में बड़ा हुआ, वहां थिएटर में सिर्फ सी-ग्रेड फिल्में लगती थीं। वही हमारी ‘सिनेमा की दुनिया’ थी। दिलीप कुमार या अमिताभ की फिल्में वहां तक पहुंचती ही नहीं थीं।”
सी-ग्रेड फिल्मों के पोस्टर, उनके बोल्ड टाइटल और थिएटर के बाहर युवाओं की लंबी कतारें — ये सब 80s और 90s के भारत की एक अनदेखी लेकिन लोकप्रिय सच्चाई रही है।
क्यों गर्मियों में छा जाती थीं सी-ग्रेड फिल्में?
एक दौर था जब मई-जून के महीने सी-ग्रेड फिल्मों के लिए ‘पसंदीदा सीजन’ माने जाते थे। इसका कारण था – स्कूलों की छुट्टियां, भीषण गर्मी और बड़े बजट की फिल्मों की अनुपस्थिति।
इन महीनों में सिंगल स्क्रीन थिएटर खाली पड़े रहते थे, तो छोटे बजट की, कामुकता से भरी फिल्मों को रिलीज किया जाता था। इन फिल्मों में लागत कम, जोखिम न्यूनतम और मुनाफा निश्चित होता था। यही वजह थी कि “जंगल लव”, “लेडी टारजन”, “जॉन मेरी मार्लो” जैसी फिल्में इसी सीजन में धड़ल्ले से रिलीज होती थीं।
सी-ग्रेड से मल्टीप्लेक्स और ओटीटी तक का सफर
समय बदला, सिंगल स्क्रीन सिनेमा बंद होने लगे, और मल्टीप्लेक्स और ओटीटी का दौर शुरू हुआ। लेकिन सी-ग्रेड फिल्मों की आत्मा अब नए लबादे में सामने आई।
महेश भट्ट जैसे निर्देशकों ने “राज़”, “जिस्म” और “मर्डर” जैसी फिल्मों के ज़रिए बोल्ड कंटेंट को नई पीढ़ी की मानसिकता और मल्टीप्लेक्स कल्चर के साथ जोड़ दिया।
अगर पहले सिल्क स्मिता ग्रामीण किरदारों में सिंगल स्क्रीन की स्टार थीं, तो अब बिपाशा बसु और मल्लिका शेरावत मेट्रो-सिटी गर्ल्स बनकर स्क्रीन पर उतरीं — अंतर सिर्फ लोकेशन और प्रेजेंटेशन का था।
‘डर्टी पिक्चर’ और ‘चमकीला’ से बदला नजरिया
जब एकता कपूर ने सिल्क स्मिता की जिंदगी से प्रेरित होकर ‘डर्टी पिक्चर’ बनाई, तो विद्या बालन की दमदार एक्टिंग और प्रजेंटेशन ने इस बोल्ड सब्जेक्ट को मुख्यधारा में ला खड़ा किया।
ठीक वैसे ही, ‘अमर सिंह चमकीला’ की कहानी को जब इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ ने पर्दे पर पेश किया, तो ‘डबल मीनिंग गायक’ की छवि एक सांस्कृतिक प्रतीक में बदल गई।
यह साफ है – कहानी वही होती है, फर्क सिर्फ नजरिए और प्रस्तुति का होता है।
तो फिल्म A-ग्रेड होगी या C-ग्रेड – तय करता है विज़न, बजट और सोच
किसी फिल्म का ‘ग्रेड’ उसके विषयवस्तु से कम और उसके बजट, प्रस्तुतिकरण और निर्देशक के दृष्टिकोण से अधिक तय होता है।
जहां बड़ी स्टारकास्ट, भव्य सेट्स और सटीक मेसेजिंग होती है, वह फिल्म A-ग्रेड कहलाती है। लेकिन जब सीमित संसाधनों में फिल्म सिर्फ उत्तेजना या सनसनी पर केंद्रित होती है, तो वह C-ग्रेड का तमगा पा जाती है।
पर सवाल ये है — क्या बदलते दौर में भी हमें “ग्रेड” के नाम पर सिनेमा की कहानी को परिभाषित करना चाहिए?
यह भी पढ़ें:
चेहरे पर काले धब्बे? ये सिर्फ झाइयां नहीं, गंभीर एलर्जी हो सकती है
 Business Sandesh Indian Newspaper | Articles | Opinion Pieces | Research Studies | Findings & News | Sandesh News
Business Sandesh Indian Newspaper | Articles | Opinion Pieces | Research Studies | Findings & News | Sandesh News